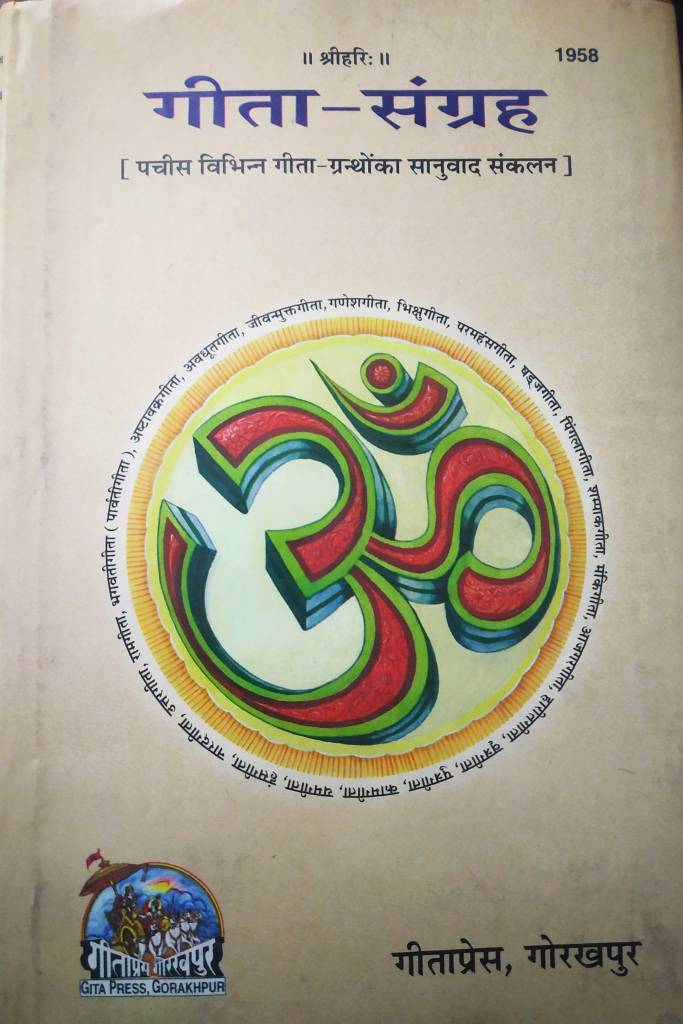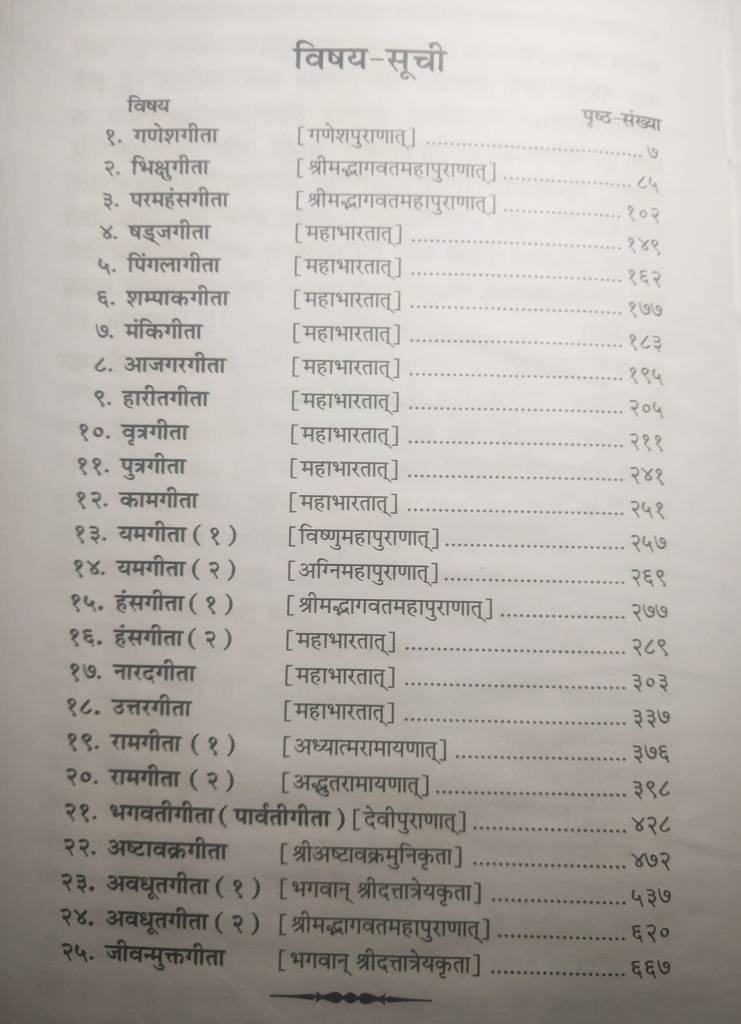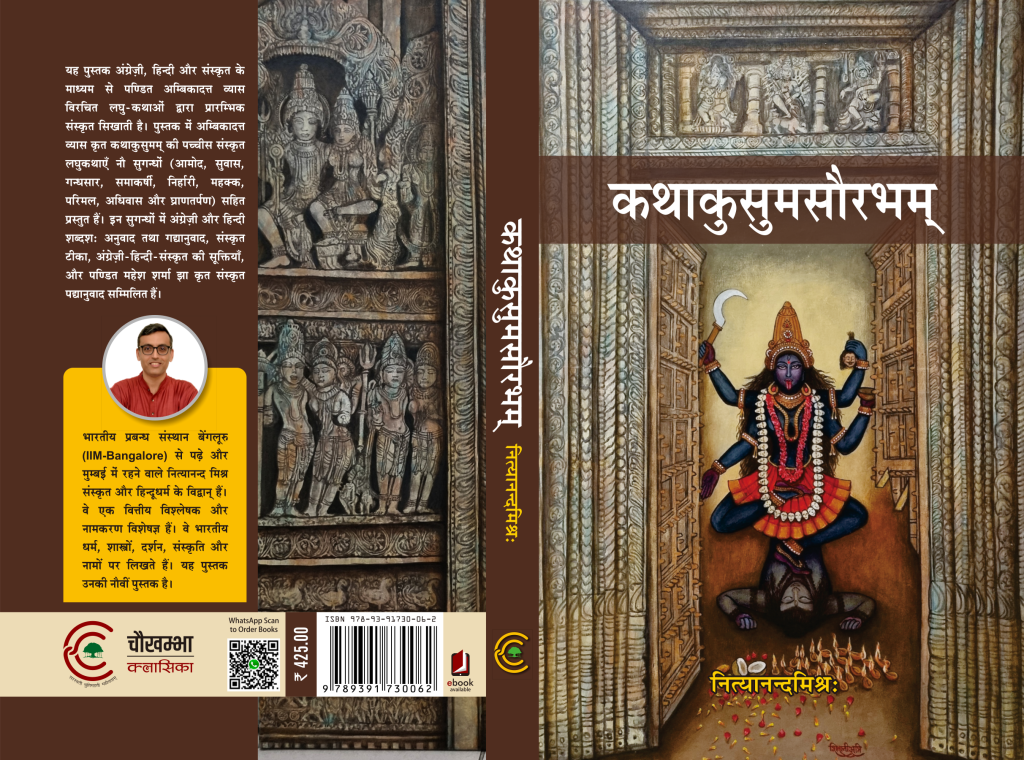https://www.academia.edu/…/JDMC_Introduction_%E0%A4%B8…
शिक्षा का वैयक्तिक स्तर पर उद्देश्य है- ‘उच्च चरित्र का निर्माण’ ताकि व्यक्ति अपना हितसाधन कर सके। सामाजिक स्तर पर इसका उद्देश्य है मनुष्य को इस प्रकार समर्थ तथा संवेदनशील बनाना कि वह समाज तथा राष्ट्र के काम आ सके। इन दोनों ही उद्देश्यों की पूर्ति व्यक्ति में अनुकूल उत्तम गुणों का विकास करके किया जा सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि हमारी शिक्षा इस लक्ष्य की ओर उन्मुख हो। पिछले अनेक दशकों से जिस प्रकार केवल भौतिक संसाधनों के अधिकाधिक दोहन की प्रक्रिया को सिखाने वाले अनुशासनों को प्राथमिकता दी गयी उससे नवशिक्षित मनुष्य ने किस प्रकार पर्यावरण सहित जीवन की अनिवार्य शर्तों का क्षरण किया है, यह हमसे छिपा नहीं है। “प्रत्यक्ष लाभ दिलाने वाले” वैज्ञानिक अनुशासनों को यदि “मानवीयता सिखाने वाले” भाषिक, साहित्यिक और मानविकी के अनुशासनों के साथ सन्तुलन में पढ़ाया नहीं गया तो आगे की स्थिति और दूभर होने वाली है। इसकी बानगी हमें मिलने लगी है। प्रतिस्पर्धा की अन्धाधुन्ध दौड़ में कोई तो ऐसा स्वर हो जो हमारे सामने जीवन और जगत् के मूलभूत प्रश्नों को उपस्थापित करे और उन प्रश्नों के उत्तर खोजने में हमारी सहायता करे। हमारी प्राचीन, मध्यकालीन भाषाओं का शिक्षण इस उपर्युक्त असन्तुलन को कम करने में हमारा सहायक इस नाते हो सकता है कि इनमें हमारे पूर्वजों का चिरसंचित और सुपरीक्षित ज्ञान सुरक्षित है। वह आज की समस्याओं के विषय में भी हमारा पर्याप्त मार्गदर्शन कर सकता है। इन विषयों की उपेक्षा हमारे लिए घातक होगी।
भारत की प्राचीन तथा मध्यकालीन भाषाओं के बीच ‘संस्कृत’ की उपस्थिति बड़े महत्त्व की है। उसकी ३ बड़ी विशेषताएँ हैं जो उसे भारत की सभ्यता तथा संस्कृति को ठीक से समझने तथा वर्तमान में उसके उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य बनाती हैं। ये हैं- संस्कृत की प्राचीनता, विपुलता तथा अविच्छिन्नता। संस्कृत वाङ्मय का प्रारम्भ वेदों से होता है जो मानवता के प्राचीनतम दस्तावेज़ हैं। हज़ारों वर्षों तक ज्ञान-विज्ञान की भाषा रहने के कारण संस्कृत में लिखा गया साहित्य विपुल है। साथ ही इसमें विविध कालों में बिना किसी बड़ी रिक्ति के ज्ञान का निरन्तर सृजन होता रहा है। भारत में मानवता की सैकड़ों पीढ़ियों ने हज़ारों वर्षों का निवेश करके जिस अनुभव सम्पदा को विभिन्न प्रकार की रचनाओं में निबद्ध किया है वे रचनाएँ संस्कृत भाषा में सुरक्षित हैं। इसलिए संस्कृत का अपनी समृद्धि के साथ सुरक्षित रहने का अर्थ है- “भारतीयों के मन में स्वदेशी भावभूमि का सुरक्षित रहना”। इस भाषा की निरन्तरता के नाते हम एक बहुमूल्य विचार प्रणाली से परिचित हो पाते हैं जो हमें एक गम्भीर साभ्यतिक बोध देता है, यह साभ्यतिक बोध है-भारतीयता का बोध। यह बोध किसी भी तरह काल अथवा देश की क्षुद्र सीमाओं में सिमटा हुआ नहीं है। इसमें व्यष्टि से लेकर समष्टि तक अस्तित्व के सभी घटकों का बराबर ध्यान रखा गया है। पाश्चात्त्य विचार प्रणाली की भाँति यह चिन्तन सरणि केवल मनुष्य को केन्द्र में नहीं रखता बल्कि मनुष्य इसमें दूसरे घटकों की तरह एक सामान्य घटक के रूप में सहजीविता के सम्बन्ध के साथ आता है।
संस्कृत द्वारा आनीत साँस्कृतिक परम्परा की मूल्यवत्ता को देश में निरन्तर समझा जाता रहा है। इसी कारण इस भाषा की सुरक्षा के निरन्तर प्रयास हमेशा जारी रहे हैं। संस्कृत के बोलचाल में होने का समय यदि २५०० वर्षों पहले (वैयाकरण पाणिनि का सम्भावित समय) का माना जाये, तो उसके बाद के समस्त भारतीय वाङ्मय को हम प्रकारान्तर से संस्कृत को बचाये रखने की प्रविधियों को खोजने और उसके प्रयोग के इतिहास के रूप में भी देख सकते हैं। पाणिनि से पहले और उनके बाद भी अनेकानेक व्याकरणों का लिखा जाना, वार्तालाप के माध्यम से संस्कृत सिखाने वाले बालावबोध पुस्तकों का प्रणयन आदि ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो उपर्युक्त कथन को प्रमाणित करते हैं। इस तरह संस्कृत शिक्षण की प्रविधियों को खोजने का एक लम्बा इतिहास रहा है। भारत में संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषाओं की परम्परा साथ में फलती-फूलती रही है। पुरानी पड़ती संस्कृत भाषा पर क्षेत्रीय प्राकृतों के उदय और विकास के कारण निरन्तर एक दबाव बना ही रहता रहा है, इसलिए उसका शिक्षण हर युग में एक चुनौती की भाँति रहा है। बदलते युग में लोगों की परिवर्तित होती मनोवृत्ति के अनुकूल नयी प्रविधियों का प्रयोग करके भारतीयों ने इस चुनौती का हर समय उत्तर दिया है। वे हमेशा से यह समझते थे कि उत्तम शिक्षक केवल वह नहीं है जो कि शास्त्रों का विपुल ज्ञान प्राप्त कर ले। यह तो उसके व्यक्तित्व की प्राथमिक और आधी योग्यता है। उसकी योग्यता तब पूर्ण होती है जब वह अपने हृदय में स्थित ज्ञान को अपने छात्रों तक ठीक ठीख पहुँचा पाता है। विक्रमोर्वशीय नाटक में कविकुलगुरु कालिदास का स्पष्ट कथन है-
श्लिष्टा क्रिया कस्यचिदात्मसंस्था संक्रान्तिरन्यस्य विशेषयुक्ता।
यस्योभयं साधु स शिक्षकाणां धुरि प्रतिष्ठापयितव्य एव ॥१.१६॥
![]() कुछ शिक्षकों ज्ञान उनके हृदय में स्थित होता है और कुछ शिक्षकों की महारत विषय को समझाने में होती है। जिस व्यक्ति में ये दोनों गुण विद्यमान है वह शिक्षकों में सबसे आगे बिठाने योग्य है।)
कुछ शिक्षकों ज्ञान उनके हृदय में स्थित होता है और कुछ शिक्षकों की महारत विषय को समझाने में होती है। जिस व्यक्ति में ये दोनों गुण विद्यमान है वह शिक्षकों में सबसे आगे बिठाने योग्य है।)
शिक्षण किस प्रकार सुगम, प्रभावी और सुसंगत हो इसके लिए निरन्तर नये रूप में विचार करना होता ही है क्योंकि हर नयी पीढ़ी बदली हुई होती है और उसके लिए पुराने, अनुपयोगी, अपरीक्षित प्रविधियों का उपयोग नहीं किया जा सकता। हमारा देश विश्व के कई अन्य देशों की तरह उपनिवेशीकरण के कठिन दौर से निकलकर आया हुआ एक देश है जो उपनिवेशीकरण की अनन्तरभावी प्रक्रिया-यूरोपीयकरण से बहुत बुरी तरह से घिरा हुआ है। यह प्रक्रिया सीधे देशज भाषाओं और संस्कृतियों पर आघात करती है। भारत में यह प्रक्रिया पिछले दशकों में और बढ़ गयी है। संस्कृत चूंकि देशज संस्कृतियों की रक्षक और देशज भाषाओं की सुरक्षा की प्रतिभूति है इसलिए पाश्चात्त्य दबावों से सबसे पहला और अधिक दुष्प्रभाव उसी पर पड़ता दीखता है। फलतः संस्कृत का शिक्षण पहले की अपेक्षा और चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। एक उदाहरण लें, आजकल की हिन्दी में अवांछित रूप से बढ़ते हुए अंग्रेज़ी के शब्दों के कारण संस्कृत पढ़ाते समय उन तत्सम शब्दों को छात्रों को नये सिरे से बताने का श्रम करना पड़ता है जो कुछ समय पहले तक हिन्दीभाषियों (या अन्य क्षेत्रीयभाषियों) के लिए सहज-सुलभ थी। यही दशा अन्य सांस्कृतिक तथा दार्शनिक संप्रत्ययों के शिक्षण की भी है। बदलते हुए समय में लोगों की प्राथमिकताएँ बदल गयी हैं क्योंकि उनकी समस्याएँ बदल चुकी हैं। इन बदलते मूल्यों वाले परिवारों में पले-बढ़े छात्र जब शिक्षकों के सामने आते हैं तो वे बिलकुल नये होते हैं। उन्हंब पुरानी तकनीकों से नहीं पढ़ाया जा सकता। उनके लिए नयी प्रविधियों का अन्वेषण करना ही होता है। यह बात किसी भी संस्कृत अध्यापक के लिए शास्त्रीय ग्रन्थों की सुरक्षा जितनी ही महत्त्वपूर्ण होनी चाहिए। दुर्भाग्यवश इस बिन्दु की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया जा पा रहा है।
ऐसे में यह देख पाना बहुत प्रसन्न करता है कि जानकी देवी मेमोरियल महाविद्यालय की युवा एवं ऊर्जस्वी संस्कृत अध्यापकों ने इस ओर एक सार्थक प्रयास किया है। उन्होंने कक्षाओं में अनेक वर्षों के अपने प्रेक्षणशील अनुभवों के आधार पर संस्कृत के विविध शास्त्रो के शिक्षण में आने वाली समस्याओं को छात्रों की दृष्टि से एकत्रित किया है, तथा उनका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करके उनके उत्तर सामने रखने का प्रयास किया है। साहित्य तथा दर्शन का अध्यापन किस प्रकार उनकी वैज्ञानिकता तथा उपयोगिता को सामने रखकर किया जा सके इसका निदर्शन भी किया गया है। निश्चित ही उनके इस प्रयास से अध्यापक समूह बड़े स्तर पर लाभान्वित हो सकेगा क्योंकि बदलते समय में शिक्षण की ये समस्याएँ सबकी साझी हैं और उनके समाधान मंा नयी प्रविधियों की खोज भी साझे प्रयासों से ही सम्भव है। इस उपक्रम को प्रारम्भ करके उसे पर्यवसान तक पहुँचाने के लिए मैं महाविद्यालय की प्रधानाचार्या तथा शिक्षक प्रभारी का विशेष धन्यवाद देता हूँ तथा सभी लेखकों का अभिनन्दन करता हूँ।
बलराम शुक्ल
संस्कृत विभाग
दिल्लओी विश्वविद्यालय